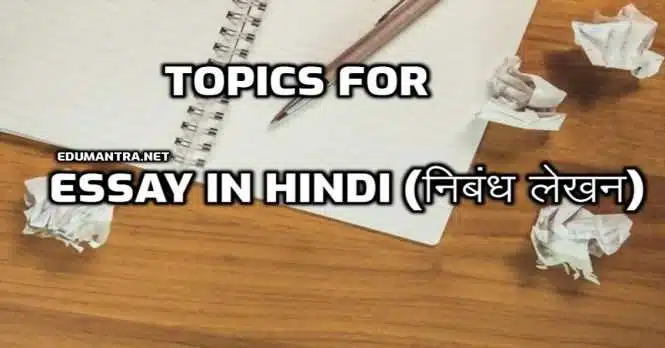
Essay in Hindi में लेखक को अपने मौलिक व्यक्तित्व एवं गागर में सागर भरने की कला का परिचय देना होता है. साथ ही हम आपको बतायेंगे Ras Kise Kahate Hain और देंगे रस से जुड़ी जानकारी उदहारण सहित.
Essay in Hindi (निबंध लेखन)
निबंध ऐसी गद्य रचना है जिसमें किसी विषय पर सीमित आकार के भीतर सुंदर ढंग से क्रमबद्ध विचार प्रकट करने का प्रयत्न किया गया हो. उत्तम निबंध रचना स्वयं में एक कला है. निबंध में लेखक को अपने मौलिक व्यक्तित्व एवं गागर में सागर भरने की कला का परिचय देना होता है. अतः निबंध लेखक को निम्नलिखित महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखनी चाहिए –
•निबंध के लिए दिए गए विषयों में से ऐसे विषय का चयन करना चाहिए जिसे आप भली-भांति समझते हों.
•निबंध – लेखन से पूर्व यह आवश्यक है कि विषय से संबंधित संपूर्ण सामिग्री जुटा ली जाए तथा उसका गंभीर मनन किया जाए.
•सामग्री एकत्र कर लेने के उपरान्त निबंध की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए.
•निबंध रचना के तीन प्रमुख तत्व हैं – (क) प्रस्तावना (भूमिका) (ख) विवेचना अथवा मध्य भाग (ग) उपसंहार अथवा अंत.
•प्रस्तावना अथवा भूमिका निबंध का महत्वपूर्ण भाग है यह भाग बहुत सशक्त, आकर्षक एवं रोचक होना चाहिए.
•विवेचना अथवा मध्य भाग लिखते समय अत्यंत सजक एवं जागरूक रहने की आवश्यकता है. इसमें अपने विचारों को विभिन्न अनुच्छेदों में विभाजित कर लेना चाहिए. प्रत्येक विचार को प्रथक – प्रथक अनुच्छेद में लिखना चाहिए.
•प्रस्तावना के समान उपसंहार भी अत्यंत प्रभावशाली होना चाहिए. निबंध का अंत इस ढंग से किया जाना चाहिए कि मुख्य भाव पाठक के मन – मस्तिष्क में गूंजता रहे.
•निबंध की भाषा शुद्ध साहित्यिक, सरल, सुबोध, प्रभावपूर्ण एवं परिमार्जित होनी चाहिए. भाषा को सशक्त बनाने के लिए यथास्थान मुहावरों एवं लोकोक्तियों का प्रयोग वांछनीय है.
•विचारों में सुसंबद्धता निबंध का अत्यावश्यक गुण है.
आजकल निबंध लेखन के लिए कोई कथन (स्टेटमेंट) दिया जाता है. उससे निबंध की दिशा तय हो जाती है. निबंध लेखक को चाहिए कि वह उस कथन को समझे. फिर एक रूपरेखा तैयार करे. विचार के कुछ बिंदु बनाए. अब निबंध लिखना सरल हो जाएगा.
Labour Essay in Hindi (भारतीय मजदूर)
भारतीय मजदूर का चित्र – दुख, दरिद्रता, भूख, अभाव, कष्ट, मजबूरी, शोषण और अथक परिश्रम – इन सबको मिला दें तो भारतीय मजदूर की तस्वीर उभर आती है.
भारतीय मजदूर की मजबूरी – कोई प्राणी खुश होकर मजदूर नहीं बनता. भारतीय मजदूर तो और भी विवश है. उनका इतना अधिक शोषण होता है कि वे मुश्किल से दो वक्त का भोजन कर पाते हैं. भारत में जनसंख्या इतनी अधिक है कि ढेर सारे मजदूर खाली रह जाते हैं. परिणाम स्वरूप मजदूरी सस्ती हो जाती है. अब सरकार मजदूरों के हितों का ध्यान रखते हुए उनका न्यूनतम वेतन तय कर देती है. इससे उन्हें काफी राहत मिलती है.
घोर परिश्रम – भारतीय मजदूर का जीवन घोर परिश्रम की कहानी है. वह मुंह अंधेरे जागता है तथा दिन – भर हाड़ – तोड़ परिश्रम करता है. प्रातः 8 से शाम 5 बजे तक अथक शारीरिक परिश्रम करने से उनका तन चूर-चूर हो जाता है. उसके पास इतनी ताकत कठिनता से बचती है कि वह आराम की जिंदगी जी सकें.
अज्ञान और अशिक्षा – अधिकांश मजदूरों के बच्चे अज्ञान और अशिक्षा में पलते हैं. मजदूर से पढ़े लिखे नहीं होते. न ही उनके पास पढ़ाई के लिए धन और अवसर होता है. इस कारण वे अज्ञान, अशिक्षा और अंधविश्वास में जीते हैं. अज्ञान के ही कारण वे पढ़े – लिखों की दुनिया में ठगे जाते हैं. डाक्टर उन्हें अधिक मूर्ख बनाते हैं. दुकानदार भी उनसे अधिक पैसे वसूलते हैं. बस या गाड़ी कहीं भी हो उन्हें सम्मानपूर्वक बैठने भी नहीं दिया जाता.
प्रसन्नता के क्षण – मजदूरों की सूखी जिंदगी में सुख के हरे – भरे क्षण तब दिखाई पड़ते हैं, जब वे रात्रि में ढोलक की ताल पर कहीं नाचते – झूमते नजर आते हैं या अपने देवता के चरणों में गान करते दिखाई देते हैं.
उत्थान के उपाय – मजदूरों की दशा में सुधार लाने के लिए अनेक मजदूर – संगठन कार्य कर रहे हैं. उनके कारण मजदूरों में नई चेतना भी आई है. अभी इस क्षेत्र में और भी सुधार होने आवश्यक हैं. इसके लिए मजदूरों को संघर्ष करना पड़ेगा.
Essay On Life in a Metropolitan City (महानगरीय जीवन)
विकास की अंधी दौड़ – महानगरों की जिंदगी के बारे में जयशंकर प्रसाद ने लिखा है –
यहां सतत संघर्ष विफलता, कोलाहल का यहां राज है.
अंधकार में दौड़ लग रही, मतवाला यह सब समाज है.
महानगरों के लोग रात को सपना लेते – लेते सोते हैं कि कल वे सोने की लंका खड़ी कर लेंगे. सुबह उठते हैं तो उचक कर उठते हैं. नाश्ता निगलते हैं और रफ्तार भरी सड़कों पर उड़न – छू हो जाते हैं. महानगरों के लोग खुद भी कमाते हैं, पत्नी भी कम आती हैं, साथ ही दो-तीन धंधे और भी करते हैं. यह बहुधन्धी लोग हमेशा कुछ लपकने, हड़पने और झपटने को तैयार रहते हैं. इन्हें दोपहिए से चार पहियों के वाहन खरीदने हैं. हवाई – मार्ग से आकाश नापना है और मौका लगते ही किसी उन्नत देश में जा बसना है. इनके जीवन में शांति नहीं, आपाधापी है. यह खाते – पीते नहीं, सपनों की अवास्तविक दुनिया में जीते हैं.
संबंधों का ह्रास – विकास क राही विकास को महत्व देता है, संबंधों को नहीं. महानगरों के बच्चे ने मामा के घर जाते हैं, न मौसी के घर. वे छुट्टियों में कोचिंग, ट्रेनिंग या पिकनिक स्पॉट पर कुछ सीखने या एन्जाय करने जाते हैं. इनके एंजॉय का अर्थ है – अपनी निजी खुशी या उपभोग. उस उपभोग में सिर्फ ‘मैं’ ही ‘मैं’ होता है. न रिश्तेदार होते हैं, न माता-पिता और न कोई और आलतू – फालतू. सचमुच वे अकेले हो जाते हैं. महानगरों का व्यक्ति अकेला हो जाता है. मां-बाप ही उसे उन्नति का मंत्र देते
25
है और वह उन्नति की राह में चलते हुए उन्हीं मां-बाप को ही वृद्ध आश्रम के हवाले कर देता है. इधर मां-बाप अकेले, उधर वह अकेला. कुंवारा है तो मित्रों का साथ, विवाहित है तो पत्नी का साथ. कुछ समय बाद न मित्र साथ, न पत्नी साथ. वह बिल्कुल अकेला रह जाता है. यह है महानगरों की जिंदगी. इसीलिए हिंदी के कवि अशोक बन्ना लिखते हैं –
मेरे दिलबर यार की बुत जैसी है शान.
अंदर तक पत्थर मगर चेहरे पर मुस्कान.
राधेश्याम शुक्ल ने इसी जड़ता से आहत होकर लिखा था –
लौटा ले मेरी सदी, अपनी सब उपहार.
पर मुझसे मत छीन तू, रिश्ते-नाते प्यार.
दिखावा – महानगरों के जीवन में प्यार नहीं, दिखावा रह गया है. हम प्रेम की कमी को उपहारों से भरना चाहते हैं. हम माता-पिता को नोट देना चाहते हैं, समय नहीं; हम बात करने को टेलीफोन देना चाहते हैं किंतु पास नहीं आना चाहते. इसलिए हमारे ड्राइंग रूम सजे रहते हैं ताकि लगे कि हम सजे – सवेरे खुशहाल हैं किंतु उन सोफों पर बैठने वाला साल में एकाध बार आता है. जैसे – जैसे हम शीशे की दीवारें, कीमती सामान, सजावटी सामग्री इकट्ठा करते जा रहे हैं, वैसे-वैसे मस्ती, लापरवाही और ठहाके कम होते जा रहे हैं.
यह महानगरीय जीवन जीवन नहीं, जीवन का आभास है. यह रेत है जो दूर से पानी का तालाब नजर आती है. इससे अच्छे हैं वे कस्बे या गांव, जहां प्यार ही प्यार पलता है. एक – दूजे के लिए जीने का संकल्प पैदा होता है.
Loktantra Mein Media ki Bhumika
लोकतंत्र में जन जागरण आवश्यक – लोकतंत्र का अर्थ है – लोकराज. लोकराज तभी संभव है, जबकि लोग जागृत हों, लोग तभी जागृत होते हैं, जब उनका समाज में सजीव संबंध हो. इस संबंध – सरोकार को निर्मित करने में पत्रकारों की भूमिका बहुत बड़ी है. प्रेस यानी सूचना – तंत्र को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा गया है. जिस देश में पत्रकार जागरूक होते हैं, उस देश का लोकतंत्र बहुत सशक्त होता है.
पत्रकार : सूचना का दूत – पत्रकार का प्रमुखतम कार्य है – सूचनाओं का आदान-प्रदान. उसकी चार आँखे और चार कान होते हैं. वह अपने आसपास घटने वाली हर घटना के प्रति चौकन्ना होता है. उसकी जिज्ञासा आम नागरिक से अधिक ठोस, स्पष्ट तथा भावुकता – रहित होती है. वह घटनाओं की भावुकता में नहीं बहता, बल्कि घटित घटना के एक-एक प्रामाणिक तथ्य की जानकारी एकत्र करता है.
पत्रकार : लोकहित को समर्पित – पत्रकार मूलतः लोक – समर्पित होना चाहिए. वह न तो स्वार्थ – प्रेरित हो, न किसी वर्ग, जाति या व्यक्ति का हित साधन करें, बल्कि जनता – जनार्दन की सेवा करें. यह बहुत कठिन कार्य है. पत्रकार के पथ पर बाधाएं आती हैं, लोभ आते हैं, जानलेवा धमकियां मिलती हैं, तो भी उसे सत्य – पथ पर बढ़ना होता है. ऐसा सत्यपंथी पत्रकार ही लोकतंत्र को सुद्रण कर सकता है.
पत्रकारिता का इतिहास ऐसे साहसी और सत्यपंथी पत्रकारों से भरा पड़ा है. गणेश शंकर विद्यार्थी जैसे पत्रकारों ने ही देश को नई रोशनी दी. उनके वचन देशवासियों के लिए प्रेरणा – स्त्रोत बने.
रचनात्मक पत्रकारिता – आजकल पत्रकारिता अश्लीलता और उत्साह के रंग में रंगती जा रही है. कोई भी समाचार पत्र या पत्रिका ऐसी नही है जिसमे अश्लील चित्र न हों. लगता है, उन्होंने अश्लीलता के सामने हार मान ली है. पत्रकार खोज – खोजकर समाज में हुई हिंसा, अपहरण, योन –लीला, भ्रष्टाचार और राजनीतिक छल को छाप रहे हैं. इससे प्रतीत होता है मानो हम नारकीय जीवन जी रहे हैं.
अनेक खोजी पत्रकार लोकतंत्र को स्वस्थ – स्वच्छ करने के नाम पर हर राजनेता के कच्चे चिट्ठे खोलने में सलंग्न रहते हैं. वे हर नेता की ऐसी गंदली
छवि प्रस्तुत करते हैं कि हमारा सभी पर से विश्वास उठ जाता है. ऐसे पत्रकार यह नहीं समझते कि इससे लोगों की राजनीति पर, नेताओं पर तथा लोकतंत्र पर आस्था नष्ट हो जाती है. पत्रकारों का काम लोकतंत्र पर आस्था जमाना, न कि उसे डिगाना.
Women’s Safety Essay in Hindi
जीवन – शैली – महानगरों की विशेषता है – भीड़ में अकेलापन. यहां लोग बहुत हैं किंतु एक – दूसरे से कटे हुए. यहां कोई किसी के लिए जीता नहीं, मरता नहीं. सभी अपनी ही धुन में जी रहे हैं. इस अकेली जिंदगी के अनेक दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं. जो कमजोर हैं, वह अकेला होकर और भी कमजोर हो जाता है. हमारे पुरुष – प्रधान समाज में नारी पहले से ही कमजोर है. महानगरों की भीड़ भाड़ में वह और भी अकेली और असहाय हो गई है.
कामकाजी महिलाओं की समस्या – कामकाजी महिलाओं की समस्या और भी गंभीर है. उन्हें हर रोज एक निश्चित समय पर बाहर निकलना पड़ता है. सुबह तो जैसे – तैसे कट जाती है वापसी के समय साँझ या रात हो जाती है. ऐसे समय में अपराधी, गुंडे और बदमाश अकेली महिलाओं की तलाश में रहते हैं. कोई उन्हें एकांत पाकर दबोच लेता है, कोई टैक्सी चालक बनकर. ऐसे में उनके मन में एक डर समा जाता है. डर के मारे से जीवन नहीं जी पातीं. अनेक बार उनके साथ बलात्कार और व्यभिचार की घटनाएं हो जाती हैं. ये घटनाएं एकाध बार नहीं होतीं. यदि किसी गुंडे के मुंह में खून लग गया तो मैं रोज – रोज बल – प्रयोग करना चाहता है. यदि महिला पुलिस में शिकायत कर दे तो भी समाधान नहीं मिलता. महिलाओं को न तो पुलिस पर भरोसा है और न पुलिस की मार खाए अपराधियों पर.
कामकाजी महिलाएं केवल सड़क पर ही असुरक्षित नहीं हैं. वे अपने आफिस में बॉस के अकेले कमरे में असुरक्षित हैं. बॉस महिलाकर्मी के अकेलेपन का फायदा उठाता है. कितनी ही महिलाओं को नौकरी के लालच में अपने बॉस की वासना का शिकार होना पड़ता है.
सुरक्षा में कर्मियों के कारण व सुझाव – महिला – सुरक्षा का सबसे चिंतनीय कारण यह है कि उन्हें विश्वास नहीं है. जो लोग महिला – सुरक्षा में लगे हैं, वे भी महिला – अत्याचार के प्रति गंभीर नहीं हैं. दूसरे, महिला सुरक्षा के लिए महिला थाने, महिला पुलिस, महिला शिकायत केंद्र, महिला वाहन चालकों की जरूरत है. रात के समय महिलाकर्मियों को घर तक छोड़ने की व्यवस्था सब जगह नहीं है. इस कारण अनेक दुर्घटनाएं हो जाती हैं.
महिला – सुरक्षा के लिए कानून बहुत सख्त होने चाहिए. महिलाओं के साथ खिलवाड़ करने वालों को कठोर दंड दिया जाना चाहिए. महिलाओं के लिए महिला – पुरुष की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए. कारखानों तथा उधोगो को बाध्य करना चाहिए कि वे महिलाओं की ड्यूटी दिन में ही रखें. यदि रात के समय ड्यूटी लेनी है तो उन्हें घर पर सुरक्षित छोड़ने की व्यवस्था करें.
सबसे बड़ा उपाय है – संस्कार. माता-पिता अपने बच्चों को नारी का सम्मान करना सिखाए. हर दुर्योधन के प्रति घ्रणा भरें, रावण के प्रति आक्रोश, और लड़कों को नारी के सम्मान की सीख दें. यदि वे लड़कियों के प्रति अनुचित व्यवहार करते हैं तो उन्हें दुत्कारें, अपमानित करें तथा समझाने – बुझाने की हर कोशिश करें.
Communalism Meaning in Hindi (सांप्रदायिकता: एक अभिशाप)
सांप्रदायिकता का अर्थ और कारण – जब कोई संप्रदाय स्वयं को सर्वश्रेष्ठ और अन्य संप्रदायों को हीन मानने लगता है, तब सांप्रदायिकता का जन्म होता है. इन्हीं अंधों को फटकारते हुए महात्मा कबीर ने कहा था –
हिंदू कहत राम हमारा, मुसलमान रहमाना.
आपस में दोउ लरै मरतु है, मरम कोई नहीं जाना.
सर्वव्यापक समस्या – सांप्रदायिकता विश्व – भर में व्याप्त बुराई है. इंग्लैंड में रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट ; मुस्लिम देशों में शिया और सुन्नी ; भारत में बौद्ध वैष्णव, शैव – बौद्ध, सनातनी – आर्यसमाजी, हिंदू – सिक्ख झगड़े उभरते रहे हैं. इन झगड़ों के कारण जैसा नरसंहार होता है, जैसी धन-संपत्ति की हानि होती है, उसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं.
भारत में सांप्रदायिकता – भारत में सांप्रदायिकता की शुरुआत मुसलमानों के भारत में आने से हुई. शासन और शक्ति के मद में अंधे आक्रमणकारियों ने धर्म को आधार बनाकर यहां के जन-जीवन को रौंद डाला. धार्मिक तीर्थों को तोड़ा, देवी-देवताओं को अपमानित किया, बहू-बेटियों को अपवित्र किया, जान- माल का हरण किया. परिणामस्वरूप हिंदू जाति के मन में उन पाप-कर्मों के प्रति गहरी घ्रणा भर गई, जो आज तक भी जीवित है. बात-बात पर हिंदू -मुस्लिम संघर्ष का भड़क उठना उसी घृणा का सूचक है.
सांप्रदायिक घटनाएं – अंग्रेज शासकों ने भी हिंदुओं और मुसलमानों – दोनों को लड़ाया. आजादी से पहले अनेक खूनी संघर्ष हुए. आजादी के बाद तो विभाजन का जो संघर्ष और भीषण नर-संहार हुआ, उसे देखकर समूची मानवता रो पड़ी. शहर-के-शहर गाजर-मूली की तरह काट डाले गए. अयोध्या के रामजन्म-भूमि विवाद ने देश में फिर से सांप्रदायिक आग भड़का दी है.
समाधान – सांप्रदायिकता की समस्या तब तक नहीं सुलझ सकती, जब तक कि धर्म के ठेकेदार उसे सुलझाना नहीं चाहते. यदि सभी धर्मों के अनुयाई दूसरों के मत का सम्मान करें, उन्हें स्वीकारें, अपनाएं, विभिन्न धर्मों के संघर्षों को महत्व देने की बजाय उनकी समानताओं को महत्व दें तो आपसी झगड़े पैदा ही न हों. कभी-कभी ईद-मिलन या होली-दिवाली पर ऐसे दृश्य दिखाई देते हैं तो एक सुखद आशा जन्म लेती है.
मदिरापान : एक सामाजिक कलंक
मदिरापान के कारण – मदिरा ऐसा नशीला पेय है, जो ऊर्जा और नशा दोनों प्रदान करता है. जो लोग उसे उर्जा के लिए पीते हैं, वे एक प्रकार से औषधि का सेवन करते हैं. इसके विपरीत जो लोग मदिरापान नशे के लिए करते हैं, वे या तो उसमें विलास का सुख देखते हैं या दुखों से बचने का उपाय ढूंढते हैं.
देखने में आता है कि मदिरापान की आदत युवा अवस्था में लगती है. लोग दोस्ती का रंग जमाने के लिए शराब पीते हैं. शराब पीकर वे मस्त हो जाते हैं. फिर वे कुछ ऐसी हरकतें भी कर देते हैं जिन्हें वे बिना शराब के न करते. इसका अर्थ है कि नशे की हालत में युवक अपने पूरे होश में नहीं रहता. वह सामाजिक मान-मर्यादा भूल जाता है. इस कारण उसे अपने समाज में बहुत बुरा -भला सुनना पड़ता है. लोग और मित्रगण शराब पिए हुए अपने मित्र से बात भी नहीं करना चाहते. इसलिए शराब एक बुराई है.
कुछ मजदूर और परिश्रमी लोग दिन भर की थकान मिटाने के लिए मदिरा का सेवन करते हैं. प्रायः वे रात्रि भोजन के बाद पीकर सो जाते हैं. ऐसे लोग उसे औषधि के रूप में लेते हैं. प्रायः वे अधिक हानि नहीं करते किंतु नशे की हालत में किसी के काम के भी नहीं रहते. एक तरह से वे परवश हो जाते हैं. ऐसे लोग भी कभी न कभी अपमानित होते हैं. यहां तक कि उनके परिवार वालों को पता होता है कि इस समय उनसे बात नहीं करनी चाहिए.
कुछ लोग शराब के आदी हो जाते हैं. वे शराब के बिना जी नहीं सकते. ऐसे लोगों के फेफड़े खराब हो जाते हैं. वे दिन-रात नशे की हालत में रहते हैं. सुबह होते ही इधर मंदिरों में भजन शुरू होते हैं, उधर वह बोतल खोल लेता है. ऐसे लोग पियक्कड़ के नाम से जाने जाते हैं.
आजकल कुछ लोग मदिरापान को प्रतिष्ठा का चिन्ह मानते हैं. जिस दावत में मदिरासेवन न हो वे उसे दावत नहीं मानते. ऐसे लोग अपने आप को बड़ा सिद्ध करने के लिए और शराब को विलास की सामग्री मानकर मदिरापान करते हैं. इस आदत की भी प्रशंसा नहीं की जा सकती. बुराई जिस भी रास्ते से आए, वह बुरी ही कहलाएगी.
पीने वालों का समाज में स्थान – शराब चाहे किसी भी कारण से पी जाए, उसे समाज में सम्मान का स्थान नहीं दिया जाता. जैसे कुल्ला करते वक्त व्यक्ति अपने छींटों को तो सहन कर लेता है किंतु किसी और के छींटे सहन नहीं कर सकता, उसी प्रकार शराबी अपनी हरकतें तो अनदेखी कर लेता है, किंतु किसी और शराबी की किसी भी प्रकार की बुरी हरकत को पसंद नहीं करता. यहां तक कि पिए हुए आदमी को भी सहन नहीं करता. कारण यह है कि नशे की हालत में उस पर किसी भी प्रकार से विश्वास नहीं किया जा सकता. वह एक प्रकार से मुसीबत होता है इसे कोई ढोना नहीं चाहता. यही कारण है कि पीने वालों की समाज में कोई इज्जत नहीं होती. उसकी किसी बात पर भी विश्वास नहीं किया जाता. कहते हैं कि वह तो शराबी-कबाबी आदमी है, उसका क्या भरोसा ? नशेड़ी पर किसी का भरोसा नहीं होता.
समाप्ति के उपाय – प्रश्न है कि मदिरापान को कैसे समाप्त किया जाए ? इसका एक ही उत्तर है – जागरूकता. मदिरापान के विरुद्ध प्रभावी ढंग से अभियान चलाया जाए. शराब पीने की बुराइयों पर फिल्में दिखाई जाएं, कविताएं लिखी जाएं, कहानियां और उपन्यास लिखे जाएं. दूसरा तरीका है सरकारों की ओर से मदिरापान पर प्रतिबंध लगाया जाए. यह भी एक प्रभावी उपाय है. परंतु देखने में आया है कि जिन प्रांतों में मदिरापान की मनाही है, वहां लोग चोरी -छिपे शराब पीते हैं. अतः यह एक सहायक उपाय है, एकमात्र उपाय नहीं.
मदिरापान रोकने का सबसे बड़ा तरीका यह है कि परिवार में बच्चों को इसके विरुद्ध मानसिक रूप से तैयार किया जाए. शराब से बचने का सर्वोत्तम उपाय है – इसका स्वाद ही न चखना. जैसे कीचड़ से दूर रहने का उपाय है – कीचड़ के संपर्क में न रहना. यदि एक बार कीचड़ में पाँव पड़ जाए तो फिर कीचड़ से घृणा कम होने लगती है. जो लोग मदिरा को हाथ न लगाने का संकल्प ले लेते हैं वे इसके दोषों से बच जाते हैं. शेष लोग तो रोज ही संकल्प लेते हैं और कल से न पीने की कसम लेकर आज पूरी बोतल पी जाते हैं.
त्योहार बनाम बाजारवाद
तात्पर्य – त्यौहार आज बाजारवाद की गिरफ्त में आ गए हैं. बाजार ने त्योहारों को अपना शिकार बना लिया है. वह त्योहारों के नाम पर अपना माल बेच रहा है. लोग भी भ्रमवश बाजार की वस्तुओं को त्योहारों का अनिवार्य अंग मान बैठे हैं. इस प्रकार त्योहार और बाजारवाद में गड़बड़झाला हो गया है. हम त्यौहार के नाम पर बाजार से वस्तुएं खरीद लाते हैं और उपभोग को ही त्यौहार का नाम दे बैठे हैं.
त्योहारों का वास्तविक स्वरूप – त्योहारों का वास्तविक स्वरूप बहुत पवित्र और पावन होता है. दशहरा इसलिए मनाया जाता है ताकि हम याद रख सकें कि बड़े से बड़े विद्वान भी नारी का अपमान करने पर घृणा का पात्र बन जाता है. दीवाली पर हम अपने पूज्य भगवान के घर आने पर खुशी मनाते हैं. होली बद नियति को जलाने की याद कराती है और भक्तों के बचने पर खुशी मनाती है. रक्षाबंधन भाई-बहन के प्यार का प्रतीक है. जन्माष्टमी भगवान कृष्ण के जन्म की याद कराती है. वैशाखी फसलों के पकने का त्यौहार है. 15 अगस्त आजादी की सांस लेने का नाम है और 26 जनवरी अपना संविधान लागू करने का त्योहार है. वास्तव में सभी त्यौहार पवित्र भाव से बने हैं और इनका स्वरूप की बहुत साधारण होता है.
दीवाली पर दिए जलाए जाते हैं. दशहरे में रावण का पुतला फूंका जाता है. होली पर लकड़ी जलाई जाती है और रंग खेले जाते हैं. राखी पर भाई को धागा बांधा जाता है. जन्माष्टमी पर मंदिर सजाए जाते हैं. 15 अगस्त को तिरंगा फहराया जाता है. 26 जनवरी को देश की प्रगति की झांकी सजाई जाती है.
बाजार का प्रभाव – बाजार की शक्तियों ने त्योहारों की मांग को देखते हुए अपना व्यापार बढ़ाने का प्रयत्न किया. दीवाली के नाम पर दीवाली पर बम –पटाखों, तरह-तरह की सजावटी लाइटों, मिठाइयों और उपचारों के ढेर लगा दिए. दीवाली के नाम पर दीवाली मेले लगाए जाते हैं. उनमें आकर्षक छूट देकर लोगों के घरों में फ्रिज, टी.वी., ए.सी., जूसर आदि पहुंचाने का प्रबंध किया जाता है. हर त्यौहार पर उपहार के पैकेटों की भरमार हो जाती है. होटल बुक हो जाते हैं. पार्टियों का फैशन चल निकलता है. करवा चौथ के नाम पर होटलों की बुकिंग शुरू हो जाती है. वैलेंटाइन डे, फादर्स डे, मदर्स डे के नाम पर करोड़ों-अरबों का कार्ड छापने का व्यवसाय चल निकलता है. प्रेम के छलावे के नाम पर उपहार की वस्तुएं खरीदी-बेची जाती हैं. वास्तव में बाजार वाले त्यौहार के नाम पर लोगों को अपना माल बेच रहे हैं और लाभ कमा रहे हैं.
दीवाली के अवसर पर हिंदुओं में इतनी मिठाईयां बांटी जाती हैं कि वे घूम-घूम कर कई हाथों से निकलने के बाद व्यर्थ से हो जाती है. धीरे-धीरे लोग इस चक्कर को समझने लगते हैं. जैसे तीर्थ पर ठगों से बचने की जरूरत होती है, उसी प्रकार त्योहारों पर बाजार के मायावी मायाजाल से भी बचने की जरूरत है.
धनहीन जीवन : एक अभिशाप
भूमिका – जीवन एक वरदान है. यह वरदान तब और भी मोहक और मूल्यवान हो जाता है जब वह साधन-संपन्न हो. धन और साधनों के बिना जीवन अपाहिज हो जाता है. नाटककार मोहन राकेश ने लिखा है – ‘दारिद्र्य वह कलंक है, जो छिपाए नहीं छिपता – केवल से छिपता ही नहीं, वह लाख-लाख गुणों को छा लेता है.’
निर्धनता का जीवन पर प्रभाव – निर्धनता मनुष्य के विकास में सबसे बड़ी बाधा है. भूखा मनुष्य दिन भर पेट भरने की जुगत में लगा रहता है. सुबह उठते ही उसे चिंता सताने लगती है कि उसका तथा उसके प्रियजनों का पेट कैसे भरेगा ? और रात होने पर फिर यही विचार मन में रहता है कि कल भोजन कैसे मिलेगा ? ऐसा व्यक्ति और किसी तरह का विकास नहीं कर सकता. आजादी, स्वाभिमान, देशप्रेम जैसे उच्च भाव उसके निकट भी नहीं आ पाते. कवि केदारनाथ अग्रवाल ने भूखे गरीब के बारे में सही लिखा है –
जो भूख मिली
सौ गुनी बाप से अधिक मिली
अब पेट खिलाए फिरता है
चौड़ा मुंह बाए फिरता है
वह क्या जाने आजादी क्या
आजाद देश की बातें क्या
निर्धन व्यक्ति का कोई चरित्र नहीं होता. वह रोटी के एक टुकड़े पर कोई भी अनचाह काम करने को बाध्य हो जाता है कविवर नीरज ने लिखा था –
भूखे पेट को देशभक्ति सिखाने वालो
भूख इंसान को गद्दार बना देती है.
निर्धनता के कारण – निर्धनता के अनेक कारण होते हैं. भारत में निर्धनता का बहुत बड़ा कारण हमारी गुलामी रही है. सैकड़ों वर्षो तक विदेशी लोगों ने यहां राज किया. वे भारत को लूट-लूट कर विदेशों में ले गए. आजाद होने पर भारत के शासकों ने भी यही किया. वे भी भारत की धन-संपदा को लूट-लूट कर या तो अपने घर भरते रहे या धन को विदेशी बैंकों में जमा करते रहे. यहां के शासक की जनता की गरीबी का कारण बन रहे.
गरीबी का दूसरा कारण है – भारत का अध्यात्म और शांति में सुखी होना. ‘मन लागो मेरे यार फकीरी में’. या ‘दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ’ – यह भाव हमे साधन-संपन्न होने से रोके रहा. तीसरे यहां धन का उचित विभाजन नहीं रहा. एक ओर अरबों, खरबों के मालिक हैं तो करोड़ों लोग रोटी के लिए भी मोहताज हैं. चौथा कारण है – यहां की असंख्य जनसंख्या. पांचवा कारण है – तकनीकी विकास पर बल न देना.
निर्धनता रोकने के उपाय – निर्धनता के जो कारण हैं, वही उसे रोकने के उपाय भी हैं. यदि भ्रष्टाचार पर कड़ाई से रोक लगाई जाए तो भारत समृद्ध हो सकता है. यदि भौतिक उन्नति को भी उचित सम्मान दिया जाए और तकनीकी विकास पर बल दिया जाए तो भारत फिर से सोने की चिड़िया बन सकता है. इसके अतिरिक्त सुशासन से धन का उचित बटवारा भी निश्चित किया जाना चाहिए.
उपसंहार – वास्तव में आज की सरकार इस दिशा में गंभीरता से प्रयत्न कर रही है. भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के काफी उपाय किए जा रहे हैं. विदेशों में जाने वाले धन का सख्त निगाह रखी जा रही है. गरीबों, किसानों और साधनहीनों के हाथों में सीधे-सीधे पैसा दिया जा रहा है. पहले जो पैसा बीच के सरकारी या अन्य अधिकारी खा जाते थे, वह पैसा अब सीधे आम लोगों के खातों में जा रहा है. इससे आम आदमी साधन-संपन्न और स्वाभिमानी बनेगा. प्रधानमंत्री ने भारत को एक मंत्र दिया है – मेक इन इंडिया. यह भारत को निर्माण के लिए प्रोत्साहित करने वाला है. आशा है कि यह उपाय भारत को धन-संपन्न बनाएंगे.
कामकाजी नारी और उसकी समस्याएं
कामकाजी नारी यानि दोहरा कार्यभार – कामकाजी नारी का अर्थ है – धनोपार्जन में लगी नारी. ऐसी नारी दुगुने संकट झेलती है. उस पर दुगुने दायित्व होते हैं. उसे घर और बाहर-दोनों के बीच संतुलन बैठाना पड़ता है. उसे रसोई, चूल्हा –चौका, सफाई, साज-सज्जा का काम तो करना ही होता है. उसके परिवार के सदस्य यह सहन नहीं कर पाते कि वह नौकरी करके पुरुषों की तरह शेष कामों से मुक्त रहे. अविवाहित कन्या के माता-पिता फिर भी अपनी बेटी के कार्यभार को बटा लेते हैं किंतु ससुराल में बहू को घर- गृहस्थी का पूरा सीन झंझट निभाना पड़ता है. परिणाम स्वरूप दुगुना काम करने को विवश हो जाती है. घर में काम से बचें तो सास नाराज, कार्यालय में कामचोरी करें तो बॉस नाराज. वह दुधारी तलवार की दोनों धारों पर चलती रहती है.
मातृत्व-काल के संकट – कामकाजी नारी को सबसे बड़ा संकट तब झेलना पड़ता है, जब वह मां बनती है. इस महत्वपूर्ण दायित्व के लिए उसे केवल चार छः महीने की छुट्टियां मिलती हैं जबकि बच्चे के लालन-पालन के लिए उसे अनेक वर्षों की आवश्यकता होती है. सच मायनों में नवजात शिशु और कामकाजी मां – दोनों नौकरी के पहिए के नीचे कुचले जाते हैं. दोनों को एक-दूसरे की सख्त जरूरत होती है. परंतु नौकरी के चलते उन्हें अनचाहे समझौते करने पड़ते हैं. बच्चे को शिशु गृहों में रखना पड़ता है. उसे मां के दूध की बजाय बाजारु दूध पिलाना पड़ता है. नारी के कामकाज की सबसे बड़ी कीमत बच्चे क्यों चुकानी पड़ती है और स्वयं नारी को भी.
कार्यालय में आने वाली बाधाएं – नारी मां बनते ही घर-गृहस्थी और बाल-बच्चों को प्राथमिकता देने लगती है. परिणामस्वरूप उसका ध्यान अपने कामकाज, व्यवसाय और नौकरी से हटने लगता है. यह बात नियोक्ता के गले नहीं उतरती. परिणामस्वरूप कामकाजी नारी को रोज-रोज अपने कार्यालय की सख्ती सहन करनी पड़ती है. प्राइवेट नौकरी पर लगी नारियां तो इस दौरान हटा दी जाती हैं.
कामकाजी नारी को कार्य के दौरान अनेक लज्जाजनक स्थितियों का सामना करना पड़ता है. उसे लोक-संपर्क के कामों में चाहे-अनचाहे लोगों से मिलना पड़ता है. यदि वह किसी एकांत-स्थल पर कार्य करती हो और उसे किसी पुरुष अधिकारी के अधीन काम करना पड़ता हो तो उसका जीवन आशंका से ग्रस्त रहता है. अनेक विवश नारियों को नौकरी के दबाव में अनचाहे समझौते करने पड़ते हैं.
समाज का असुरक्षित वातावरण – हमारे समाज का असुरक्षित वातावरण भी कामकाजी नारी की समस्याओं को बढ़ावा देता है. कामकाजी नारी को नौकरी के काम से कभी-कभी देर-सवेर हो जाती है. तब एकांत-स्थान अंधेरा और घर की दूरी-तीनों मिलकर उसकी धड़कनें बढ़ा देते हैं. ऐसी स्थिति में उसके साथ कुछ भी अपमानजनक घट सकता है.
परिवार का असहयोग – कामकाजी नारी के साथ सबसे बड़ी समस्या यह है कि उसके परिवार-जन उसे नौकरी तो करवाना चाहते हैं किंतु उसके बदले उसे सुविधा या सहयोग नहीं देना चाहते. उसके पतिदेव घर के कामों में हाथ बटाना अपना अपमान समझते हैं. सास- ननद उसके साथ रुखाई से पेश आती हैं. बच्चे मां पर पूरा अधिकार रखकर हर काम पूरा होता देखना चाहते हैं. उधर समाज के सदस्य भी नारी की नौकरी को ईर्ष्या और उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं. इस कारण उसके पग-पग पर अनेक संकट खड़े दिखाई देते हैं.
ओलंपिक खेलों में सुधार के उपाय
ओलंपिक में भारत की दयनीय स्थिति – ब्राजील के रियो शहर में हुए ओलंपिक खेलों में भारत ने जो शर्मनाक प्रदर्शन किया है वह पूरे विश्व को हैरत में डालने वाला है. 125 करोड़ की आबादी वाले देश को अनुपात के हिसाब से कम से कम 80 पदक जीतने चाहिए थे. परंतु भारत ने जीते केवल 2 पदक. वे भी रजत और कांस्य. सोने का एक भी पदक भारत की झोली में नहीं आ सका. हमारे 119 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया जिसमें अनेक खिलाड़ी पहले भी पदक प्राप्त कर चुके थे फिर भी स्थिति दयनीय रही.
कारण – खेलों में भारत की दुर्दशा के कारणों पर विश्लेषण करें तो सबसे बड़ा कारण नजर आता है भारत का खेलों के प्रति तिरस्कार. हमारे यहां एक कहावत प्रचलित है –
पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब. खेलोगे कूदोगे होगे खराब.
जिस देश में खेलों के प्रति यह हीन भावना हो, वहाँ खेल कैसे पनप सकते हैं. भारत में खेलना-कूदना अपना समय खराब करना माना जाता है. जो लोग अपने भविष्य के प्रति बहुत सजग हैं, वे अपने जीवन का एक-एक क्षण धन कमाने के नुस्खों को अपनाने में लगे रहते हैं. यहां खेलों में पैसा है नहीं. इसलिए माता-पिता अपने बच्चों को खेलों से कोसों दूर रखते हैं. विद्यालय भी खेलों को व्यक्तित्व निर्माण के लिए आवश्यक नहीं मानते. उधोग और सरकारी प्रतिष्ठान नौकरी देते समय बच्चे के स्वास्थ्य की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं देते. परिणामस्वरूप बच्चों को खेलने की प्रेरणा कहीं से नहीं मिलती. वे खेलते हैं तो केवल अपने शौक के कारण खेलते हैं.
सुधार के उपाय – भारत में खेलों की स्थिति में सुधार तब लाया जा सकता है, जबकि इसे आजीविका या कैरियर से जोड़ा जाए. खिलाड़ियों को नौकरियाँ और सम्मान दिये जाएँ. उन्हें खेलों में मस्त रहने के कारण अन्न-जल के लिए न तरसना पड़े. इसके लिए सरकार को खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए उपाय करने होंगे. विद्यालयी शिक्षा में खेलों को अनिवार्य करना होगा. इससे खेल- शिक्षकों और कोचों के पद बनेंगे. तब ढेर सारी नौकरियां देखकर बहुत से प्रतिभाशाली खिलाड़ी खेलों में अपना भविष्य मानकर उसे अपनाएगें. तब माता-पिता भी उन्हें खेलों के प्रति प्रोत्साहित करेंगे. ऐसी स्थिति में ढेर सारी प्रतिभाएं उभर कर सामने आएंगी. अब भी खिलाड़ियों और पहलवानों को पुलिस, सेना और अन्य रक्षात्मक क्षेत्रों की नौकरियां दी जाती है, परंतु अभी ये बहुत कम है.
खेल-संस्कृति का विकास – भारत में क्रिकेट के खेल-संस्कृति है. यहां गली-गली में, गांवों और नगरों में, मैदानों और सड़कों पर भी क्रिकेट देखी जा सकती है. यहां क्रिकेट के खिलाड़ियों को फिल्मी सितारों जैसा सम्मान दिया जाता है. इसलिए यहां क्रिकेट का वातावरण है. बड़े-बड़े उद्योगों और वित्तीय संस्थानों ने क्रिकेट को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. यही भूमिका अन्य खेलों को भी मिलनी चाहिए. इसके लिए क्रिकेट के मोह को कुछ हद तक कम करके खेलों को उत्सव की तरह से खेलना होगा.
जिस तरह से प्रति 4 वर्ष बाद ओलंपिक होते हैं, उसी तरह प्रति 4 वर्ष बाद शीतकालीन ओलंपिक भी होते हैं. जो अगला शीतकालीन ओलंपिक 1922 में टोक्यो में है. उसमें बर्फ पर खेले जाने वाले खेल होते हैं, जिसमें से कुछ है स्कीईंग, आईस स्केटिंग आदि.
गर्म देश होने के कारण इन खेलों की सुविधा भारत में बहुत कम है. इसलिए ये खेल भारत में अत्यंत कम लोकप्रिय है.
राजनीति से दूरी – खेलों के विकास में राजनीति भी बहुत बड़ी बाधा है. भारत में जितने भी खेल-संसाधन हैं, उनके अध्यक्ष नामी खिलाड़ी न होकर राजनेता हैं. इस कारण श्रेष्ठ खिलाड़ी उचित स्थान नहीं ले पाते. रियो ओलंपिक में सुशील कुमार को लेकर जो विवाद छिड़ा, वह दुर्भाग्यपूर्ण है. राजनेता खेलों में कम रुचि लेते हैं और अपने मनमानी चलाने और अध्यक्ष पद की कुर्सी की खींचतान में अधिक रुचि लेते हैं. इस कारण खेलों को हानि होती है. यदि विश्वविद्यालयों की तरह खेल संसाधनों को भी खिलाड़ियों के सुपुर्द किया जाए तो खेलों में अद्भुत सुधार हो सकता है.
क्रिकेट मैच का आंखों देखा वर्णन
कहाँ, कैसे, कब – क्रिकेट का 12वां विश्वकप मैच. 16 जून, 2019 को इंग्लैंड के मैनचेस्टर स्थित ओल्ड ट्रैफर्ड स्टेडियम में भारत और पाकिस्तान के बीच मैच खेला गया. आसमान में उमड़ते-घुमड़ते बादल. दोनों टीमों में जबरदस्त उत्साह. इन जबरदस्त प्रतिद्वंदियों को देखने के लिए लोगों में इतना उत्साह था कि सारी टिकटें एक ही मिनट में ऑनलाइन बिक गईं.
आनंददायक – भारत-पाकिस्तान जब आमने-सामने होते हैं तो जबरदस्त आनंद होता ही है. सबकी नजर चौकों-छक्कों, कैचों – विकेटों पर होती है. इस बार टास पाकिस्तान ने जीता. फिर-भी उनके कप्तान सरफराज अहमद ने गेंदबाजी चुनी. पाकिस्तान को अपनी तेज गेंदबाजी पर विश्वास था तो भारत को ठोस बल्लेबाजी पर. भारत की बांछें खिल गई.
कप्तान विराट कोहली ने राहुल और रोहित शर्मा को सलामी बल्लेबाज के रूप में उतारा. उन्होंने एकाध ओवर संभलकर खेला. दूसरे ओवर में रोहित ने एक चौका लगाया. चौथे ओवर में एक और चौका. पांचवें ओवर में एक चौका और छक्का. इस प्रकार 12वें ओवर में 34 गेंदों पर अर्द्धशतक और 29वें ओवर में शतक ठोक दिया. दोनों ओपनर्स ने 136 रन की साझेदारी की. इसके बाद आए कप्तान विराट कोहली. दोनों ने पाकिस्तान की बखिया उधेड़ दी. पाकिस्तान के आमिर को छोड़कर और कोई गेंदबाज भारत के बल्लेबाजों को रोक नहीं पाया. रोहित शर्मा ने शानदार 140 रन की पारी खेली. वे राकेट शॉट खेलने के चक्कर में कैच हो गए. इसके बाद आए हार्दिक पांड्या ने धुआंधार पारी खेली. बीच में बारिश के कारण मैच रुक गया. अंततः भारत ने 5 विकेटों पर 336 का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया.
परिणाम – पाकिस्तान के लिए यह विशाल स्कोर एक पहाड़ था जिसे पार करना कठिन था. पांचवें ही ओवर में गेंदबाज भुवनेश्वर के पांवों में मोच आ गई और वे पैवेलियन से बाहर चले गए. उनकी जगह पर गेंदबाज के रूप में आए विजय शंकर ने पहली ही गेंद पर पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज को एल.बी.डब्ल्यू. आउट कर दिया. भारत को पहली बार सफलता मिली. उसके बाद फखर और बाबर ने 104 रनों की लंबी पारी खेली किंतु उनका रन-औसत कम था. मैच धीरे-धीरे भारत के पाले में गिरता चला जा रहा था. उसके बाद पाकिस्तान के विकेट गिरने शुरू हुए. उधर बरसात के आसार बनने लगे. स्थिति यह हो गई कि मुझे विजय शंकर, हार्दिक पांड्या और कुलदीप यादव के होते पाकिस्तान के 129 रनों पर 5 विकेट चले गए. इस बीच बारिश आ गई. डी.एल.एस. नियम के चलते पाकिस्तान को 40 ओवरों में 302 रन बनाए थे किंतु वह रन नहीं बना पाई. इस प्रकार भारत ने पाकिस्तान से यह वर्ल्ड-कप मैच भी जीत लिया और अजेय का अजेय बना रहा.
भारत-पाकिस्तान का यह मैच दर्शकों के लिए इतना रोमांचक था कि जर्मनी, अमेरिका, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और भारत से असंख्य दर्शक यहाँ मैच देखने आए थे. मैच शुरू होने से पहले सड़कों पर भी ‘भारत माता की जय’ और ‘जीवे-जीवे पाकिस्तान’ के नारे लग रहे थे. स्टेडियम के अंदर पाकिस्तानी और भारतीय प्रशंसकों के अपने-अपने समूह थे. इनमें भी आपसी होड़ थी जिसमें भारतीय प्रशंसक पाकिस्तानी प्रशंसकों पर भारी पड़ रहे थे. इस प्रकार यह मैच एक अविस्मरणीय मैच था जिसे भुलाया नहीं जा सकता. रोहित शर्मा इस मैच का नायक था.
पर्यटन का महत्व
पयर्टन का आनंद –
सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ ?
जिंदगानी गर रही तो मौजवानी फिर कहाँ ?
जीवन का असली आनंद घुमक्कड़ी में है ; मस्ती और मौज में है. प्रकृति के सौन्दर्य का रसपान अपनी आंखों से उसके सामने उसकी गोद में बैठकर ही किया जा सकता है. उसके लिए आवश्यक है – पर्यटन.
पर्यटन के लाभ – पयर्टन का अर्थ है – घूमना. बस घूमने के लिए घूमना. आनंद -प्राप्ति और जिज्ञासा-पूर्ति के लिए घूमना. ऐसे पैटर्न में सुख ही सुख है. ऐसा पयर्टक दैनंदिन की भारी-भरकम चिंताओं से दूर होता है. जो व्यक्ति इस दशा में जितनी देर रहता है, उतनी देर तक वह आनंदमय जीवन जीता है.
पयर्टन का दूसरा लाभ है – देश-विदेश की जानकारी. इससे हमारा ज्ञान समृद्ध होता है. पुस्तकीय ज्ञान उतना प्रभावी नहीं होता जितना कि प्रत्यक्ष ज्ञान. पयर्टन से हम देश-विदेश से खान-पान, रहन-सहन तथा सभ्यता-संस्कृति की जानकारी मिलती है. इससे हमारे मन में बैठे हुए कुछ अंधविश्वास टूटते हैं. हमें यह विश्वास होता है कि विश्व भर का मूल रूप से एक है. हमारी आपसी दूरियां कम होती हैं. मन उदार बनता है. पूरा देश और विश्व अपना-सा प्रतीत होता है. राष्ट्रीय एकता बढ़ाने में पयर्टन का बहुत बड़ा योगदान है.
पयर्टन : एक उद्योग – वर्तमान समय में पर्यटन एक उद्योग का रूप धारण कर चुका है. हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर आदि पर्वतीय-स्थलों की अर्थ-व्यवस्था पयर्टन पर आधारित है. वहां वर्षभर विश्व-भर में पयर्टक आते हैं और अपनी कमाई खर्च करते हैं. इससे ये पयर्टक-स्थल फलते-फूलते हैं. वहां के लोगों को आजीविका का साधन मिलता है.
पयर्टक के प्रकार – पर्यटक-स्थल अनेक प्रकार के हैं. कुछ स्थल प्राकृतिक सौंदर्य के लिए विख्यात हैं. जैसे – प्रसिद्ध पर्वत-चोटियाँ, समुंद्र-तल, वन-उपवन. कुछ पयर्टक-स्थल धार्मिक महत्त्व के हैं. जैसे – हरिद्वार, वैष्णो देवी, काबा, कर्बला आदि. कुछ पयर्टक-स्थल ऐतिहासिक महत्व के हैं. जैसे – लाल-किला, ताजमहल आदि. कुछ पयर्टन-स्थल वैज्ञानिक, सांस्कृतिक या अन्य महत्व रखते हैं. इनमे से प्राकृतिक सौंदर्य तथा धार्मिक महत्व के पयर्टन-स्थलों पर सर्वाधिक भीड़ रहती है.
वृक्षारोपण की आवश्यकता
भूमिका –
धरती पर ये वृक्ष हैं जैसे सिर पर केश I
इनके कारण दीखता, हरा-भरा परिवेश II
धरती की शोभा वृक्षों से है. एक हरी-भरी पहाड़ी देखिए और एक नंगा बूचा पहाड़ देखिए. आपको स्वयं ही वृक्षों की महिमा का बोध हो जाएगा. वृक्ष धरती के श्रृंगार हैं, उसके कवच हैं.
आवश्यकता – वृक्ष केवल श्रृंगार ही नहीं है अपितु धरती की आवश्यकता हैं. ये धरती की देह पर उगे हुए नलकूप हैं जो आकाश और बादलों से पानी को पीते हैं तथा धरती की कोख को हरा-भरा रखते हैं. यदि ये न हो तो धरती बाँझ हो जाए. उसके जल-भंडार सूख जाएं. धरती फट जाए. यह हरा-भरा जीवन नष्ट हो जाए. धरती पर जल है तो फसलें हैं. फसलें हैं तो अरबों – अरबों .लोग जीवित हैं जल है तो जीवन है. ये वृक्ष जल के बड़े स्रोत हैं.
लाभ – भविष्यपुराण में लिखा है – जिसकी संतान नहीं है, उसके लिए वृक्ष की संतान है. ये वृक्ष संतान की तरह मनुष्य की सेवा करते हैं. वृक्ष लगाना दस गुणवान पुत्रों से भी अधिक लाभकारी बताया गया है. वृक्षों के लाभ ही लाभ हैं. यह हमें छाया देते हैं, फल-फूल देते हैं, अनेक औषधियां देते हैं, हमारी उच्छिष्ट वायु को भी पी जाते हैं और अपनी देह से शुद्ध वायु छोड़ते हैं. एक प्रकार से ये हमारे प्राण दाता हैं. वृक्ष तो ऐसे देवता हैं जो मरते-मरते भी हमारे घर-रसोई रोशन कर जाते हैं. या तो इनकी लकड़ी हमारे खिड़की-दरवाजों की शोभा बनती हैं, या हमारे लिए भोजन बनाती हैं. और नहीं तो शमशान तक भी हमारा साथ देती हैं और हमें संसार से सम्मान पूर्वक विदा करती है.
मनुष्यों के वृक्षों के प्रति कर्तव्य – वृक्ष कुछ नहीं मांगते. ये केवल अपने जीवन के लिए दो गज जमीन मांगते हैं. आप जल दे दें तो ठीक, वरना वातावरण से अपने लिए धूप-नमी सोख ही लेते हैं. धरती की सतह पर 33% जंगल होने चाहिए. तभी धरती का सन्तुलन बना रह सकता है. दुर्भाग्य से मनुष्य ने जंगलों को काट-काट कर अपने लिए कंकड़-पत्थर के निर्माण खड़े कर लिए. इसलिए धरती का पर्यायवरण बिगड़ गया. असमय बाढ़ें, तूफान, सूखा, गर्मी, प्रदूषण बढ़ने लगे.
आज हम मनुष्यों का कर्तव्य है कि हम फिर-से धरती पर वृक्ष उगाएं. वृक्षों की कमी को पूरा करें. हर व्यक्ति जीवन में कम से कम एक वृक्ष अवश्य लगाए. लगाए ही नहीं, उसका पालन-पोषण करे. जैसे स्वच्छता अभियान चला है, वैसे ही वृक्षारोपण अभियान चले. सड़कों के किनारे, गलियों में, पार्कों में वृक्ष लगाए जाएं.
निष्कर्ष – वृक्ष लगाना हमारा सहज कर्तव्य है. यह जीवन की मांग है. हमारा कोई भी अनुष्ठान वृक्षों के बिना पूरा नहीं होता. ऐसे देवतास्वरूप वृक्ष का सम्मान करना सीखें.
वन और हमारा पर्यावरण
वन और पर्यावरण – वन और पर्यावरण का गहरा संबंध है. ये सचमुच जीवन दायक हैं. ये वर्षा लाने में सहायक होते हैं और धरती की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाते हैं. वन ही वर्षा के धारासार जल को अपने भीतर सोखकर बाढ़ का खतरा रोकते हैं. यहीं रुका हुआ जल धीरे–धीरे सारे पर्यावरण पुनः चला जाता है. वनों की कृपा से ही भूमि का कटाव रुकता है. सूखा कम पड़ता है तथा रेगिस्तान का फैलाव रुकता है.
प्रदूषण निवारण में सहायक – आज हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या है – पर्यावरण-प्रदूषण. कार्बन डाइऑक्साइड, गंदा धुआँ, कर्ण भेदी आवाज, दूषित जल -इन सबका अचूक उपाय है – वन-संरक्षण. वन हमारे द्वारा छोड़ी गई गंदी सांसो को, कार्बन डाइऑक्साइड को भोजन के रूप में ले लेते हैं और बदले में हमें जीवनदायी आक्सीजन प्रदान करते हैं. इन्हीं जंगलों में असंख्य, अलभ्य जीव जंतु निवास करते हैं जिनकी कृपा से प्राकृतिक संतुलन बना रहता है. आज शहरों में लगातार ध्वनि-प्रदूषण बढ़ रहा है. वन और वृक्ष ध्वनि-प्रदूषण भी रोकते हैं. यदि शहरों में उचित अनुपात में पेड़ लगा दिए जाएं तो प्रदूषण की भयंकर समस्या का समाधान हो सकता है. परमाणु ऊर्जा के खतरे को तथा अत्यधिक ताप को रोकने का सशक्त उपाय भी वनों के पास है.
वनों की अन्य उपयोगिता – वन ही नदियों, झरनों और अन्य प्राकृतिक जल -स्त्रोतों के भंडार हैं. इनमें ऐसी दुर्लभ वनस्पतियां सुरक्षित रहती हैं जो सारे जग को स्वास्थ्य प्रदान करती हैं. गंगा-जल की पवित्रता का कारण उसमें मिली वन्य औषधियाँ ही हैं. इसके अतिरिक्त वन हमें लकड़ी, फल, फूल-पत्ती, खाद्य-पदार्थ, गोंद तथा अन्य सामान प्रदान करते हैं.
वन-सरंक्षण की आवश्यकता – दुर्भाग्य से आज भारत वर्ष में केवल 23% वन रह गए हैं. अंधाधुंध कटाई के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है. वनों का संतुलन बनाए रखने के लिए 10% और अधिक वनों की आवश्यकता है. जैसे- जैसे उद्योगों की संख्या बढ़ती जा रही है, वाहन बढ़ते जा रहे हैं, वैसे-वैसे वनो की आवश्यकता और अधिक बढ़ती जाएगी.
प्राकृतिक आपदा: कारण और निवारण
प्राकृतिक आपदा के प्रकार – प्राकृतिक आपदा का अर्थ है – प्रकृति की ओर से आए संकट. यह धरती, जिसे मनुष्य अपनी भाषा में आपदा यह संकट कहता है, वास्तव में धरती की व्यवस्था है. पहाड़ों का टूटना, समुद्र का अनियंत्रित होना, तूफान आना, बाढ़ें आना, भूकंप आना – ये प्रकृति की अंगड़ाइयां हैं. निरंतर घूमती हुई पृथ्वी जब भी करवट लेती है तो बड़े-बड़े भूकंप आते हैं.
और हमारी बनाई हुई हरी-भरी दुनिया को उजाड़ देती है. वास्तव में पृथ्वी पर हुए निर्माण और विनाश उसकी स्वाभाविक लीलाएं हैं. हमें उन लीलाओं को समक्ष सिर झुका कर ही चलना चाहिए. ऐसा दिन कभी नहीं आएगा, जब कि मानव सारे प्राकृतिक संकटों पर काबू पा लेगा.
उत्तराखंड का जलप्रलय – कुछ दिनों पहले भारत के उत्तराखंड में जलप्रलय आया. पहाड़ों पर बादल फटे. घनघोर बारिश हुई. 16 जून रात सवा आठ बजे और 17 जून सुबह 6 बजे ऐसे दो सैलाब आए कि भारत के करीब एक लाख पयर्टक पहाड़ों में फँस गए. जो जहां था, वहीं जलप्रलय का शिकार हो गया. किसी की कार-बस में कीचड़ घुस आया, किसी का वाहन जल के वेग में बह गया. कोई होटल या धर्मशाला में बैठे-बैठे उस सैलाव में बह गया. उस होटल में ही उसकी जल-समाधि हो गई. आज तक पता नहीं चला कि वे नदी में बहते हुए मकान से बाहर भी निकल सके या मकान समेत बाढ़ में बह गए. किसी के ऊपर चट्टान आ गिरी तो किसी के पांव के नीचे से धरती खिसक गई. हजारों यात्री तत्काल काल की भेंट चढ़ गए.
कारण – इस भयंकर जल-शैलाब को लेकर देश-भर में चर्चा शुरू हो गई कि इस प्राकृतिक आपदा का मूल कारण क्या है. पर्यावरण के जानकार कहते हैं कि हमने अपनी अंधाधुन प्रगति की चाह में जिस प्रकार पहाड़ों को काटा है, उनकी छाती में सुरंगें बनाई हैं, बारुद लगाकर विस्फोट किए हैं, उन पर चलने के लिए सड़कें बनाई हैं, उससे पहाड़ों में खलबली मच गई है. भू-स्खलन आम हो गए हैं. पहाड़ों पर सदियों से जमे हुए पत्थर, पेड़ और मिट्टी अपनी जड़ों से उखड़ गई है. इस कारण कोई भी प्राकृतिक तूफान आता है तो भयंकर विनाश छा जाता है. यह सब मानव की करतूत है. हम प्रकृति को छोड़ेंगे तो प्रकृति अपने हिसाब से हमसे बदला लेगी. पहाड़ों पर बनाए जाने वाले बाँध तो बहुत बड़ा खतरा है.
प्रश्न यह है कि क्या मनुष्य को इन प्राकृतिक आपदाओं से मुक्ति मिल सकती है इसका उत्तर है – नहीं. वह दिन कभी नहीं आने वाला जबकि हम सभी प्राकृतिक आपदाओं से मुक्त हो जाएंगे. परंतु हमारी समझ में प्राकृतिक छेड़छाड़ के जो-जो कारण हमें हानि पहुंचा रहे हैं. हम उन पर नियंत्रण कर सकते हैं. महात्मा गांधी ने कहा था – यह प्रकृति करोड़ों क्या अरबों – अरबों लोगों का पालन बड़े आराम से कर सकती है किंतु एक भी इनसान की तृष्णा पूरी नहीं कर सकती.
निवारण के उपाय – हमें महात्मा गांधी के इस संदेश को जीवन में उतारना होगा. अपनी हवस को पूरा करने के लिए वृक्षों को काटना, पहाड़ों को काटना, झीलें बनाना, बांध बनाना बंद करना होगा. शेष सब पशु-पक्षी के प्राकृतिक प्रकृति की चिंता किए बिना जीवन जी रहे हैं. हम भी अपनी तृष्णाओं पर नियंत्रण रखें. जिस काम में खतरा महसूस हो, कम से कम उससे बचे. फिर भी हमें आवश्यक कार्यवाही करनी पड़े तो पहले सुरक्षा के उपाय अपनाएं.
मानव जीवन के लिए यह भी आवश्यक है कि हम प्राकृतिक आपदा आने पर उससे निबटने के उपाय हमेशा तैयार रखें. आग लगने पर कुआं खोदने में कोई समझदारी नहीं है.
आपदाएं कभी समय देकर नहीं आतीं. वे बिना बताए कभी भी, कहीं भी आ सकती हैं. इसलिए हमें सब जगह आपदा-प्रबंधन के उपाय सँवार करके रखने होंगे. तभी हम मौत के किसी भी जलजले से बच सकते हैं.
श्रम का महत्व
संसार में आज जो भी ज्ञान-विज्ञान की उन्नति और विकास है, उसका कारण है परिश्रम – मनुष्य परिश्रम के सहारे ही जंगली अवस्था से वर्तमान विकसित अवस्था तक पहुंचा है. उसने श्रम से खेती की. अन्न उपजाया, वस्त्र बनाएं. घर, मकान, भवन, बाँध, पुल, सड़कें बनाई. पहाड़ों की छाती चीरकर सड़कें बनाने, समुंद्र के भीतर सुरंग खोदने, धरती के गर्भ से खनिज-तेल निकालने, आकाश की ऊंचाइयों में उड़ने में मनुष्य ने बहुत परिश्रम किया है.
परिश्रम करने में बुद्धि और विवेक आवश्यक – परिश्रम केवल शरीर की क्रियाओं का ही नाम नहीं है. मन तथा बुद्धि से किया गया परिश्रम भी परिश्रम कहलाता है. एक निर्देशक, लेखक, विचारक, वैज्ञानिक केवल विचारों, सलाहों और युक्तियों को खोजकर नवीन आविष्कार करता है. उसका यह बौद्धिक श्रम भी परिश्रम कहलाता है.
परिश्रम से मिलने वाले लाभ – परिश्रम का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इससे लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता मिलती है. दूसरे, परिश्रम करने वाला मनुष्य सदा सुखी रहता है. उसे मन ही मन प्रसन्नता रहती है कि उसने जो भी भोगा, उसके बदले उसने कुछ कर्म भी किया. महात्मा गांधी का यह विश्वास था कि ‘जो अपने हिस्से का काम किए बिना ही भोजन पाते हैं, वे चोर हैं.’
परिश्रमी व्यक्ति का जीवन स्वाभिमान से पूर्ण होता है, जबकि ऐय्याश दूसरों पर निर्भर तथा परजीवी होता है. परिश्रमी स्वयं अपने भाग्य का निर्माता होता है. उसमें आत्मविश्वास होता है. जबकि विलासी जन सदा भाग्य के भरोसे जीते हैं तथा दूसरों को मुंह ताकते हैं.
उपसंहार – वेदवाणी में कहा गया है – ‘बैठने वाले का भाग्य भी बैठ जाता है और खड़े होने वाले का भाग्य भी खड़ा हो जाता है. इसी प्रकार सोने वाले का भाग्य भी सो जाता है और पुरुषार्थी का भाग्य भी गतिशील हो जाता है. चले चलो, चले चलो.’ इसीलिए स्वामी विवेकानंद ने सोई हुई भारतीय जनता को कहा था – ‘उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको.’ श्रम ही मनुष्य के हाथ में है, परिणाम नहीं. अतः श्रम अवश्य करो. इसी से मनुष्य को आत्मसंतोष प्राप्त हो सकता है.
विपत्ति कसौटी जो कसे सोई सांचे मीत
जीवन की सरसता के लिए मित्र की आवश्यकता – ‘मित्रता’ का तात्पर्य है – किसी के दुख-सुख का सच्चा साथी होना. सच्चे मित्रों में कोई दुराव-छिपाव नहीं होता. वे निश्चल भाव से अपना सुख-दुख दूसरे को कह सकते हैं. उनमें आपसी विश्वास होता है. विश्वास के कारण ही वे अपना ह्रदय दूसरे के सामने खोल पाते हैं. मित्रता शक्तिवर्धक औषधी के समान है. मित्रता में नीरस काम भी आसानी से हो जाते हैं. दो मित्र मिल कर दो से ग्यारह हो जाते हैं.
जीवन-संग्राम में मित्र महत्त्वपूर्ण – मनुष्य को अपनी जिंदगी के दुख बांटने के लिए कोई सहारा चाहिए. मित्रता ही ऐसा सहारा है. एडिशन महोदय लिखते हैं – ‘मित्रता खुशी को दूना करके और दुख को बाँटकर प्रसन्नता बढ़ाती है तथा मुसीबत कम करती है.’
सच्चे मित्र की परख और चुनाव – विद्वानों का कहना है कि अचानक बनी मित्रता तो सोच-समझकर की गई मित्रता अधिक ठीक है. मित्र को पहचानने में जल्दी नहीं करनी चाहिए. यह काम धीरे-धीरे धैर्यपूर्वक करना चाहिए. सुकरात का वचन है – ‘मित्रता करने में शीघ्रता मत करो, परंतु करो तो अंत तक निभाओ.’
मित्रता समान उम्र के, समान स्तर के, समान रूचि के लोगों में अधिक गहरी होती है. जहाँ स्तर में असमानता होगी, वहां छोटे-बड़े का भेद होना शुरू हो जाएगा. सच्ची मित्रता वही है जो हमें कुमार्ग की ओर जाने से रोके तथा सन्मार्ग की प्रेरणा दे. सच्चा मित्र चापलूसी नहीं करता. मित्र के अवगुण पर परदा भी नहीं डालता. वह कुशलता-पूर्वक मित्र को उसके अवगुणों से सावधान करता है. उसे सन्मार्ग पर चलने में सहयोग देता है.
सच्चा मित्र मिलना सौभाग्य की बात – यह सत्य है कि सच्चा मित्र हर किसी को नहीं मिलता. विश्वासपात्र मित्र एक खजाना है जो किसी-किसी को ही मिलता है अधिकतर लोग तो परिचितों की भीड़ में अकेले रहते हैं. दुःख – सुख में उनका कोई साथी नहीं होता. जिस किसी को अपना एक सह्द्र मित्र मिल जाए, वह स्वयं को सौभाग्यशाली समझे.
मन के हारे हार है, मन के जीते जीत
मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति : मन – मानव की सबसे बड़ी शक्ति ‘मन’ है. मनुष्य के पास मन है, इसलिए वह मनुष्य है, मनुज है, मानव है. मानसिक बल पर ही मनुष्य ने आज तक की यह सभ्यता विकसित की है. मन मनुष्य को सदा किसी न किसी कर्म में रत रखता है.
मन के दो पक्ष : आशा-निराशा – धूप-छांव के समान मानव-मन के दो रूप हैं – आशा-निराशा जब मन में शक्ति, तेज और उत्साह ठाठें मारता है तो आशा का जन्म होता है. इसी के बल पर मनुष्य हजारों विपत्तियों में भी हंसता-मुस्कुराता रहता है. निराश मन वाला व्यक्ति सारे साधनों से युक्त होता हुआ भी युद्ध हार बैठता है. पांडव जंगलों की धुल फांकते हुए भी जीते और कौरव राजसी शक्ति के होते हुए भी हारे. अतः जीवन में विजयी होना है तो मन को शक्तिशाली बनाओ.
मन की विजय का अर्थ – मन की विजय का तात्पर्य है – काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जैसे शत्रुओं पर विजय. जो व्यक्ति इनके वश में नहीं होता, बल्कि इन्हें वश में रखता है, वह पूरे विश्व पर शासन कर सकता है. स्वामी शंकराचार्य लिखते हैं. – ‘जिसने मन को जीत लिया उसने जगत को जीत लिया .’
मन पर विजय पाने का मार्ग – गीता में मन पर नियन्त्रण करने के दो उपाय बताए गए हैं – अभ्यास और वैराग्य. यदि व्यक्ति रोज-रोज त्याग या मोह- मुक्ति का अभ्यास करता रहे तो उसके जीवन में असीम बल आ सकता है.
मानसिक विजय ही वास्तविक विजय – भारतवर्ष ने विश्व को अपने मानसिक बल से जीता है, सैन्य बल से नहीं. यही सच्ची विजय भी है. भारत में आक्रमणकारी शताब्दियों तक लड़-जीत कर भारत को अपना न बना सके, क्योंकि उनके पास नैतिक बल नहीं था. शरीर बल से हारा हुआ शत्रु फिर – फिर आक्रमण करने आता है, परंतु मानसिक बल से प्राप्त हुआ शत्रु स्वयं इच्छा के चरणों में लोटता है. इसीलिए हम प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं –
हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें.
दूसरों की जय से पहले, खुद को जय करें.
जब आवै संतोष धन, सब धन धूरि समान
तृष्णा का दुख – महात्मा गांधी लिखते हैं – ‘यह वसुंधरा अपने सारे पुत्रों को धन – धान्य दे सकती है, किंतु ‘एक’ भी व्यक्ति की तृष्णा को पूरा नहीं कर सकती.’ यह पंक्ति अत्यंत मार्मिक है. इसे पढ़कर यह रहस्य उद्घाटित होता है कि मनुष्य का असंतोष उसकी समस्याओं का मूल है. उसकी प्यास कभी शांत नहीं होती. शरीर तृप्त होने पर भी मन तृप्त नहीं होता.
दुख का कारण – वासनाएं – मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक विभिन्न वस्तुओं के पीछे पागल हुआ घूमता है. कभी उसे खिलौने चाहिए, कभी खेल, कभी धन चाहिए, कभी यश, कभी कुर्सी चाहिए, कभी पद. इन सबके आकर्षण का कारण है – इनकी प्यास. मनुष्य इस प्यास को त्याग नहीं सकता. इसके प्यास के मारे वह जीवनभर इनकी गुलामी सहन करने को तैयार हो जाता है. वास्तव में उसकी गुलाबी का कारण उसका अज्ञान है. उसे पता ही नहीं है कि वस्तुओं में रस नहीं है, अपितु, इच्छा और इच्छा-पूर्ति में रस है. जिस दिन उसे अपने इस मनोविज्ञान का बोध हो जाएगा, तब भी उससे यह गुलामी छोड़ी नहीं जा सकेगी, क्योंकि इच्छाएं अभुक्त वेश्याएं हैं जो मनुष्य को पूरी तरह पी डालती हैं और फिर भी जवान बनी रहती है.
वासनाओं का समाधान – इस प्रश्न का उत्तर गीता में दिया गया है – ज्ञान वैराग्य और अभ्यास से मन की वासनाओं को शांत किया जा सकता है. जब वस्तुएं व्यर्थ हैं तो उन्हें छोड़ना सीखें. सांसारिक पदार्थ जड़ हैं, नश्वर हैं आसान सारी तो उनकी जगह चेतन जगत को अपनाना सीखे. परमात्मा का ध्यान करें. मन बार-बार संसार की ओर जाए तो साधनापूर्वक, अभ्यासपूर्वक उसे परमात्मा की ओर लगाएं. इन्हीं उपायों से मन में संतोष आ सकता है. संतोष से स्थिरता आती है. और स्थिरता से आनन्द मिलता है. वास्तविक आनन्द भी वही है जो स्थिर हो, चंचल न हो. सांसारिक सुख चंचल है, जबकि त्यागमय आनंद स्थायी है. अतः यह सच है कि ‘जब आवै संतोष धन, सब धन धूरि समान.
करत-करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान
अभ्यास से निपुणता – महान उपलब्धि पाने के दो साधन है – प्रतिभा और अभ्यास. प्रतिभा ईश्वर की देन होती है. उस पर हमारा वश नहीं होता. अभ्यास मनुष्य के वश में है. इसके बल पर वह बड़ी-से-बड़ी सफलता पा सकता है. प्रतिभावान लोगों को भी अभ्यास करना पड़ता है. लता मंगेशकर और सचिन तेंदुलकर महान प्रतिभाएं हैं. इन्हें भी प्रदर्शन से पहले कड़े अभ्यास में से गुजरना पड़ता था. लताजी कहती हैं – वे स्टूडियो में गाना रिकॉर्ड करने से पांच मिनट पहले तक भी अभ्यास करना नहीं छोड़ती. सचिन तेंदुलकर विश्व के महानतम बल्लेबाज होते हुए भी मैच से पहले नेट पर अभ्यास अवश्य किया करते थे.
अभ्यास हमारी कला को साधता है. वह हमारे गुरु को और अधिक उत्कर्ष पर पहुंचा देता है और कमियों को दूर कर देता है. जिस गेंद को खेलने में खिलाड़ी को परेशानी होती है, उसे अभ्यास द्वारा ही दूर किया जा सकता है. कोई कितना भी अच्छा तैराक हो, अभ्यास से ही वह सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकता है. इसी प्रकार जो विद्यार्थी हर प्रश्न का उत्तर लिख-लिखकर देख लेता है, वह परीक्षा भवन में आत्मविश्वास से बैठता है. वास्तव में अभ्यास से निपुणता आती है और निपुणता से आत्मविश्वास आता है तभी व्यक्ति सफलता प्राप्त करता है.
कठिन कार्य भी अभ्यास से संभव – हवा में कलाबाजी दिखाते हुए, लड़ाकू विमानों को कालाबाजारी दिखाते हुए, पर्वतारोहियों को खड़ी चट्टानों पर चढ़ते हुए, पैराशूटिंग करते हुए, समुंद्र की छाती पर छोटी सी नाव दौड़ाते हुए, हजारों फुट की ऊंचाई से छलांग
लगाते हुए मन में भय उत्पन्न होता है और लगता है कि यह असंभव कार्य है. इसे मैं नहीं कर सकता. सर्कस के करतबों को देखकर भी भय लगता है. रेल की पटरी पर मीलो दौड़ते हुए, मलखंब पर नाचते कूदते हुए देखकर जमीन पांव के नीचे से खिसक जाती है. परंतु जब कोई व्यक्ति अभ्यास करने लगता है तो ये कुशलतायें उसकी मुट्ठी में कैद होने लगती हैं. सोचिए, नवजात शिशु सोच भी नहीं सकता कि वह भी कभी उठकर बैठेगा और दौड़ेगा. किंतु निरंतर अभ्यास से वही शिशु बड़े होकर आश्चर्यचकित कर देने वाले कारनामे दिखलाता है. यह सब निरंतर अभ्यास से संभव है.
अभ्यास का महत्व – विश्व के प्रसिद्ध मुक्केबाज को उसके मित्र ने अनजाने में उसके चेहरे पर पंच कर दिया. मुकेश से इसका जबड़ा टूट गया. उपचार के बाद मित्र ने पूछा – दोस्त ! यह कैसे हुआ ? तुम तो भीषण-से-भीषण मुक्केबाजों के धांसू मुक्कों को भी सह जाते हो. फिर कहां मैं और कहां मेरा मरियल-सा मुक्का ! मुक्केबाज बोला – बात है तैयारी की. मैं तुम्हारे मुक्के के लिए तैयार नहीं था. जब मैं अभ्यास से अपने आपको मुक्के सहने के लिए तैयार कर लेता हूं. तो बड़े से बड़े आघात भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाते.
वास्तव में अभ्यास ही सबसे बड़ा गुरु है. वह मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति को भी विद्वान बना देता है. जब अभ्यास से एक रस्सी पत्थर पर भी निशान छोड़ देती है. तो मानव क्या नहीं कर सकता ? सब जानते हैं कि अर्जुन को भी मात देने वाला एकलव्य द्रोणाचार्य की सीख से नहीं, बल्कि अभ्यास की महिमा से कुशल धनुर्धर बना था. इसलिए किसी ने कहा है – सफलता के तीन मंत्र हैं – अभ्यास, अभ्यास और अभ्यास.
जहां चाह वहां राह
कहावत का भाव, चाह से तात्पर्य – ‘जहां चाह, वहां राह’ एक कहावत है. इसका तात्पर्य है – जिसके मन में चाहत (इच्छा) होती है, उसके लिए वहाँ रास्ते अपने – आप बन जाया करते हैं. ‘चाह’ का अर्थ है – कुछ करने या पाने की तीव्र इच्छा.
सफलता के लिए कर्म के प्रति रुचि और समर्पण – सफलता पाने के लिए कर्म में रूचि होना अत्यंत आवश्यक है. जो लोग केवल इच्छा करते हैं किंतु उसके लिए कुछ करना नहीं चाहते. वे ख्याली पुलाव पकाना चाहते हैं. उनका जीवन असफल होता है. सफल होने के लिए कर्म के प्रति समर्पण होना चाहिए. जयशंकर प्रसाद ने लिखा है –
ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है
इच्छा क्यों पूरी हो मन की.
एक दूसरे से न मिल सकें
यही बिडंबना है जीवन की.
कठिनाइयों के बीच मार्ग-निर्माण – कर्म के प्रति समर्पित लोग रास्ते की कठिनाइयों से नहीं घबराया करते. कविवर खंडेलवाल के शब्दों में –
जब नाथ जल में छोड़ दी
तूफान ही में मोड़ दी.
दे दी चुनौती सिंधु को
फिर पार क्या, मंझधार क्या.
वास्तव में रास्ते की कठिनाइयां मनुष्य को चुनौती देती हैं. वे युवकों के पौरुष को ललकारती हैं उसी में से कर्मवीरों को काम पूरा करने की प्रेरणा मिलती है. इसलिए कठिनाइयों को मार्ग निर्माण का साधन मानना चाहिए.
कोई उदाहरण सूक्ति – देश को स्वतंत्रता कैसे मिली ? गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग क्यों किया ? अंग्रेजी को शासन ने उन्हें चुनौती दी. गांधी के मन में आया कि सरकार का विरोध किया जाए. उन्होंने अपने स्वभाव के अनुसार सत्य और अहिंसा के पथ पर रहते हुए विरोध किया. अंग्रेजों की डिग्रियां फाड़ डाली. भारत में आकर नमक कानून तोड़ा. भारत छोड़ो आंदोलन चलाया. परिणाम यह हुआ कि सारा भारत जाग उठा. एक दिन भारत स्वतंत्र हो गया.
निष्कर्ष – इस कहावत से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि प्रबल इच्छा शक्ति को मन में धारण करो. वह इच्छा शक्ति अपने-आप रास्ते तलाश लेगी. इच्छा-शक्ति वह ज्वालामुखी है जो पहाड़ों की छाती फोड़कर भी प्रकट हो जाती है.
सफलता की कुंजी : मन की एकाग्रता
मन की एकाग्रता क्यों – मनुष्य ‘मन’ के अनुसार चलता है. वह मन को साधने से ही ‘मुनि’ बनता है इसी मन को एक बिंदु पर टिकाने से शक्ति का उदय होता है. जिस प्रकार सूरज की धूप को लेंस द्वारा एकाग्र करने पर कागज जल जाता है. उसी प्रकार मन को एकाग्र करने पर अद्भुत प्रभाव उत्पन्न होता है. कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद किसी भी पुस्तक को कुछ ही मिनटों में पढ़ डालते थे. जब उनसे इसका रहस्य पूछा जाता था तो वे कहते थे –मन की एकाग्रता ही इसका रहस्य है. कोई निशानेबाज तभी सफल होता है जबकि उसकी लक्ष्य पर दृष्टि अचूक होती है. कोई क्रिकेटर तभी छक्का मारता है जबकि उसकी गेंद पर पैनी दृष्टि होती है. कोई गेंदवाज तभी विकेट लेता है जबकि उसे केवल और केवल विकेट्स दिखाई देती हैं. कोई कैच तभी हो पाती है जबकि फील्डर अपना संपूर्ण ध्यान गेंद की गति पर रखता है. मन की एकाग्रता आवश्यक है.
सतत अभ्यास – प्रायः लोगों का मन भटकता रहता है कटी पतंग की तरह. कभी घर, कभी बाजार, कभी क्रिकेट, कभी फिल्म, कभी पढ़ाई, कभी पिकनिक तो कभी गपशप. वे मन को बांधकर एक लक्ष्य पर स्थिर नहीं कर पाते. गीता में उसका एक उपाय बताया गया है – सतत अभ्यास. निरंतर अभ्यास करने से ध्यान की एकाग्रता बढ़ती है और सफलता भी प्राप्त होती है. रहीम ने भी कहा है –
करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान.
रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान.
यदि विद्यार्थी का मन अपने विषय पर टिकता नहीं है तो क्या करें ? क्या उस विषय को छोड़ दें और मन को जहां चाहे भटकने दें ? नहीं. वह अपने मन को द्रण करें कि उसे विषय को समझना ही है. तब उसकी एकाग्रता अपने आप तीव्र हो जाएगी. जैसे बाजार के शोर-शराबे के बीच भी व्यक्ति पैसे का हिसाब ठीक-ठीक रखता है. उसे निश्चित पैसे चुकाना और शेष पैसे लेना याद रहता है. वह अनमना होकर पैसे गिनना नहीं भूलता. यदि एकाध बार भूल जाए तो उसे फिर फिर गिनता है और अंततः ठीक हिसाब कर ही लेता है. इसी प्रकार अपने मन को प्रयासपूर्वक एकाग्र किया जा सकता है.
सफलता की कुंजी – रहीम ने लिखा है –
एकै साधै सब सधै, सब साधै सब जाय.
यदि सफलता पानी है तो मन को एक ही लक्ष्य पर केंद्रित करो. द्रोणाचार्य की भाषा में कहें तो चिड़िया की आंख पर केंद्रित करो. फिर न चिड़िया दिखाई दे, न टेहनी, न पेड़, और न धरती-आकाश. ऐसा तीर ठीक लक्ष्य पर लगेगा. जो व्यक्ति निरंतर भटकते रहते हैं, वे कहीं नही पहुँचते. रेलवे स्टेशन पर खड़ा यात्री यदि गाड़ियाँ बदलता रहे तो कहीं नहीं पहुंचेगा. यदि निश्चित गाड़ी पर सवार हो जाये तो अपने लक्ष्य पर देर-सवेर अवश्य पहुंचेगा. यही सफलता – सूत्र है.
बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए
सोच-विचार कर काम का लाभ – इस सृष्टि का नियम है कि हर काम के साथ हानि और लाभ दोनों जुड़े रहते हैं. हर काम एक श्रंखला की बात दूसरे कर्म से भी जुड़ा होता है. इसलिए किसी एक काम को करने के बाद उसका अंत नहीं हो जाता. उसके परिणाम बहुत बाद तक मिलते रहते हैं. अतः व्यक्ति को हर काम सोच-समझ कर करना चाहिए. उसका परिणाम-दुष्परिणाम सोचकर ही करना चाहिए. यदि किसी को सामने होता अन्याय देखकर क्रोध आ गया तो बिना सोचे-समझे उसमें कूद नहीं पड़ना चाहिए. यदि आपको परीक्षा-भवन में कोई मुफ्त में नकल की पर्ची थमा दे तो बिना सोचे-समझे उसे थाम नहीं लेना चाहिए. आपके ध्यान में यह बात आनी चाहिए कि दूसरों के झगड़ों में कूदने से एक ओर आप दोनों को भला कर सकते हैं और पुण्य के भागीदार बन सकते हैं. दूसरी ओर, इससे आपको यातनाएं भी सहनी पड़ सकती हैं.
जीवन में कुछ काम रेल की पटरी की तरह होते हैं जिन पर एक बार पैर रख दिया तो फिर बहुत दूर तक उस दिशा में जाना ही पड़ता है. अतः पढ़ाई के लिए विषय चुनते समय, काम-धंधा चुनते समय, जीवन-साथी चुनते समय और बच्चों का भविष्य तय करते समय बहुत सावधानी बरतनी चाहिए. सचिन तेंदुलकर ने बचपन में ही तय कर लिया कि उसे क्रिकेट खेलनी है. परिणामस्वरूप उसे सफलता हाथ लगी. लेकिन जिस विद्यार्थी में खेल के प्रति रुचि और कौशल नहीं है, सचिन की राह पर नहीं चल सकता. उसे अपने –आप को देखना होगा. अपनी शक्तियों को तौलना और आंकना होगा. तभी वह ठीक दिशा को चुन पाएगा और हानि के बजाय लाभ प्राप्त करेगा.
बिना विचारे करने से हानियां – बिना सोचे-विचारे काम करने से समय नष्ट होता है. स्टेशन पर खड़ा आदमी यदि बिना सोचे-समझे किसी गाड़ी में चढ़ गया और बाद में पता चला कि यह तो उल्टी दिशा में जा रही है तो उसे हानि के अतिरिक्त कुछ नहीं मिलेगा. बहुत से विद्यार्थी बिना लक्ष्य के पढ़ते चले जाते हैं. 12-15 वर्ष पढ़ने के बाद पता चलता है कि उनकी डिग्री का कोई मूल्य नहीं है. उसके बल पर कोई नौकरी नहीं मिलती. नौकरी मिलती है तो उसमें उसकी रूचि नहीं बनती. परिणामस्वरूप या तो उसे बहुत-सा समय खराब करके फिर से कोई दूसरी दिशा पकड़नी पड़ती है या फिर जीवन-भर उस काम को बेमन होकर घसीटना पड़ता है. परिणामस्वरूप जीवन में खिलावट नहीं आ पाती. धन की बोरियां चाहे भर जाए किंतु प्रसन्नता का डिब्बा खाली रह जाता है. यह बात अपराध, भ्रष्टाचार, नशाखोरी जैसे बुरी आदतों की ओर पैर रखने में होती है. यदि एक बार किसी कन्या गलत राह पकड़ ली और युवक ने चोरी-चकारी का एक कारनामा कर दिया तो फिर से उसे कारावास या अंडरवर्ल्ड में धँसना ही पड़ता है. अतः पहले ही कदम पर सोच-विचार कर लेना चाहिए.
पश्चाताप से बचें – जीवन में बहुत बार गलत कदम उठ जाते हैं. उनके कारण धन, समय और प्रतिष्ठा को बहुत ठेस लगती है. परंतु बीती हुई गलतियां पर पछतावा करने से कुछ हाथ नहीं आता. पछतावा करना अंधेरे को पीटना है. अंधेरे की लाठी से कितना भी पीटो, उजाला नहीं मिलता. उजाला पाने की एक राह है ; जब भी ठीक मार्ग का बोध हो जाए, गलत मार्ग को त्याग दो और उचित मार्ग की ओर चल दो. तभी से जीवन में पुनः प्रसन्नता लौट आएगी. इसलिए कहा गया है – सुबह का भूला शाम को वापस लौट आए तो उसे भटका हुआ नहीं कहते.